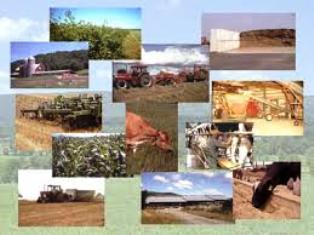इन कृषि मशीनों से कृषि को बनाये आसान और करें कृषि की लागत को कम
कृषि मशीनों के प्रयोग से उत्पादकता को बढाया जा सकता है | भारत वर्ष में कुल जोत का लगभग 63% क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित है जिससे 42 – 44 % खाधान्न उत्पादन की प्राप्ति होती है और लगभग 500 मिलियन (35 % आबादी) लोगों का पेट भरता है बारानी क्षेत्रों में येसी फसलें लेते है जो कम वर्ष या सिंचाई की स्थिति में उग सकें |
खेती की समस्याएं :
अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा तथा इसका असामान्य वितरण, वर्षा का देर से आना व जल्दी ख़त्म होना, फसल के दौरान लम्बी सूखा अवधि, मृदा में कम जलधारण क्षमता, कम मृदाउर्वरा, शक्ति, उन्नत तकनीक की कमी, पशुओं का कम उत्पादन व चारे की कमी, संसाधनों की कमी आदि |
धान, मक्का, कोंदों, राई, सरसों, मूंगफली एवं दलहनी फसलें उत्तर प्रदेश के बारानी क्षेत्रों में उगाते हैं | इन क्षेत्रों में पैदावार भी कम होती है | अधिक पैदावार लेने के लिए नमी संरक्षण, समय पर उर्वरक प्रयोग, समय से बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, उचित भूमि उपयोग, जलागम प्रबंधन तथा बारानी खेत के अन्य तरीके अपनाना आवश्यक है | इसके अतिरिक्त आजकल अनेक उन्नत कृषि यंत्र शोध संस्थनों द्वारा विकसित किये गये हैं जिनके प्रयोग से किसानों को लाभ होता है तथा 12 – 34 % तक उत्पादन में वृधि होती है |
कृषि मशीनीकरण : मुख्य तकनिकी
फर्टीसीडड्रिल
फर्टीसीडड्रिल के प्रयोग से 20% तक बीज तथा 15 – 20 % तक उर्वरक की बचत होती है | फसल सघनता में 5 – 20% तक वृधि होती है | किसान की कुल आय में 30 – 50% तक बढ़ोत्तरी होती है | भूमि विकास, जुताई एवं खेती की तैयारी हेतु निम्नलिखित यंत्रों का उपयोग होता है |
जीरो टिलेज मशीन
जीरो टिलेज मशीनसे बगैर जुताई किए गेंहू व अन्य फसलों की बुवाई करते हैं | इस मशीन के प्रयोग से लगभग रु. 2000 – 3000 प्रति हेक्टेयर तक लागत में कमी आती है |
पशु चालित पटेला हैरो
पशु चालित पटेला हैरो ढेले तोड़ने, ठूंठ या घासपात इक्टठा करने, खेत को समतल करने हेतु बुवाई से पूर्व प्रयोग किया जाता है | इससे 58% खेत की तैयारी वाले खर्चे में कमी आती है, 20% श्रम की बचत होती है तथा 3 – 4% तक पैदावार में वृधि देशी हल से जुताई करने की तुलना में होती है |
ट्रैक्टर चालित डिस्क हैरो
ट्रैक्टर चालित डिस्क हैरो का उपयोग बगीचों, पेड़ों के बीच अच्छा होता है | इससे 40 % तक श्रम तथा 54% खेत की तैयारी की लागत कम आती है | पैदावार में 2% तक वृधि पुराने तरीके की तुलना में प्राप्त होती है |
डक – रुक कल्टीवेटर
डक – रुक कल्टीवेटर काली मिटटी कड़ी परत वाली भूमि में कम गहराई की जुताई करने में अच्छा कार्य करता है | इससे 30% श्रम की बचत, 35% परिचालन कीमत में कमी तथा 30% तक पैदावार में वृधि पशुचालित कल्टीवेटर की तुलना में होती है |
रोटावेटर
रोटावेटर से सीडबैड शुष्क व नमीयुक्त भूमि तैयार किया जाता है | इससे हरी खाद वाली फसलों एवं खेत में पड़े भूसा आदि को मिटटी में अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है | इससे मिटटी भुरभुरी हो जाती है | इससे 60% श्रम की बचत होती है तथा ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 2% पैदावार बढ़ती है |
ट्रैक्टर चालित सबस्वायलर
ट्रैक्टर चालित सबस्वायलर भूमि की कड़ी परत को तोड़ने, मिटटी का ढीली करने तथा पानी को नीचे रिसने में मदद करता है | इससे छोटी – छोटी नाली भी बनाई जा सकती है जो की पानी के निकास के लिए प्रयोग हो सकती है | इसके उपयोग से 30% तक पैदावार में वृधि हो सकती है क्योंकि गहरी जुताई से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है |
धान – ड्रम सीडर
से धान के पहले से जमे हुए बीजों को सीधे रूप से लेवा खेत में बोया जाता है | इससे 20% तक बीज की बचत होती है तथा हाथ से खरपतवार निकालने में पंक्तियों में बुवाई के कारण मदद मिलती है |
पशुचालित प्लान्टर, ट्रैक्टर चालित फर्टीसीडड्रिल, ट्रैक्टर चालित धान बुवाई यंत्र, बहुफसली सीडड्रिल एवं प्लान्टर, मूंगफली खुदाई यंत्र, मूंगफली थ्रैसर, मूंगफली दाना निकालने का यंत्र, मक्का छिलाई यंत्र, सूरजमुखी थ्रैसर, कम्बाइनड हार्वेस्टर आदि नविन यंत्र विकसित किये गये है जिन्हें प्रयोग कर कृषि उत्पादन में वृधि की जा सकती है |